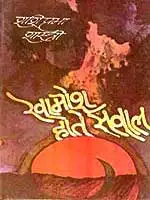|
नारी विमर्श >> खामोश होते सवाल खामोश होते सवालशशिप्रभा शास्त्री
|
360 पाठक हैं |
|||||||
एक नारी की सशक्त और योजनाबद्ध जीवन जीने की चाह क्या कर सकती है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मन को नियोजित पद्धति से भी चलने के लिए बाध्य किया जा सकता है। योजनाबद्ध ढंग से ही खामोश होते सवाल की नायिका अनुराधा ने क्रांति की है। अनर्गल सामाजिक मान्यताओं से जूझती,कर्तव्य-पथ पर चलती-बढ़ती अनुराधा ने अपने बच्चों और अपने स्वच्छंदताप्रिय पति के लिए भी रास्ता उरेहा है। अलग-थलग रहते हुए भी उनके लिए सुख-सुविधाएँ जुटाई हैं-श्वसुर का संपूर्ण दायित्व तो आरंभ से ही उस पर था, उसके लिए विष-वपन करनेवाली स्थितियों का जन्म इसी से हुआ। प्रस्तुत उपन्यास मे लेखिका की सशक्त लेखनी द्वारा रचित यह असमान्य नारी-गाथा निश्चित ही अद्भुत और स्पृहणीय हैं।
दो शब्द
व्यक्ति जन्मजात न अच्छा होता है, न बुरा, बस वह तो मनुष्य होता है।
स्थितियाँ ही उसे भला-बुरा बनाती हैं, जबकि अपने आचरण का दोष वह माता-पिता
या अपने किसी अन्य गुरुजन पर डालता है। अपनी चारित्रिक विशेषताओं के लिए
दरअसल वह स्वयं उत्तरदायी है और उत्तरदायी हैं उसकी परिस्थितियाँ, जो उसे
नियति द्वारा निर्धारित रास्तों पर चलने के लिए लाचार बना देती हैं, अपनी
तमाम कोशिशों के बावजूद वह उस मार्ग पर बढ़ता चलता है, जिसकी उसने कभी
कल्पना भी नहीं की होती।
इस प्रकार के व्यक्ति को उसकी स्थिति का बोध करवाने की क्षमता और अधिकार वही व्यक्ति रखता है, जो संबंधित व्यक्ति को अपना माने और खुले दिल से उसकी खामियों को दरकिनार करता हुआ, उसे सही रास्ते पर लाने की चाहना रखे, अपना कर्तव्य समझे।
कुछ ऐसी ही स्थितियों से जूझती चली है यह कथा, जो एकांगी या किसी एक व्यक्ति की कहानी न होकर बड़े सामाजिक सरोकारों से ग्रथित है, इसकी सार्थकता पाठकीय मनोतल द्वारा इसके तंत को पकड़ पाने में ही निहित है।
इस प्रकार के व्यक्ति को उसकी स्थिति का बोध करवाने की क्षमता और अधिकार वही व्यक्ति रखता है, जो संबंधित व्यक्ति को अपना माने और खुले दिल से उसकी खामियों को दरकिनार करता हुआ, उसे सही रास्ते पर लाने की चाहना रखे, अपना कर्तव्य समझे।
कुछ ऐसी ही स्थितियों से जूझती चली है यह कथा, जो एकांगी या किसी एक व्यक्ति की कहानी न होकर बड़े सामाजिक सरोकारों से ग्रथित है, इसकी सार्थकता पाठकीय मनोतल द्वारा इसके तंत को पकड़ पाने में ही निहित है।
शशिप्रभा शास्त्री
एक
बचपन से सुनती आई हूँ कि आत्मकथा लिखना आसान काम नहीं है, इसके लिए लेखक
को काफी साहसी और कलम का धनी होना चाहिए। मैं जानती हूँ, मुझमें ऐसा कुछ
नहीं है, फिर भी मैं लिखने बैठी हूँ; कम-से-कम मेरे पास घटनाएँ हैं, कई
हादसों से मैं गुजर चुकी हूँ, जिनकी याद मुझे अक्सर उद्धेलित करती रहती
है। लिखने के लिए क्या यही काफी नहीं है-घटनाएँ और उन्हें कलम से पुरोने
की अदम्य लालसा ?
नहीं, आत्मकथा लिखने के लिए मेरे विचार में एक तीसरी चीज और जरूरी है, ईमानदारी और सचाई। लोग प्रायः अपने को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं, जो कुछ हुआ है, उसे मोड़-तोड़कर रखने की कोशिश करते हैं जिससे वे सुर्खरू भी बने रहें और आत्मकथा लिखने जैसी ख्याति भी अर्जित कर लें-अपनी यह आपबीती खुलकर लिखने में मुझे कोई दरेग नहीं है, मैं ऐसा कोई बड़ा व्यक्तित्व भी तो नहीं, जिसे समाज का भय हो, फिर उन घटनाओं को घटित हुए भी आज अर्सा बीत गया है, अपने इस नए जीवन में प्रविष्ट हुए भी मुझे आठ वर्ष से ऊपर हो गए हैं, मैं अब पूरी पक्की गृहस्थिन हो चुकी हूँ; फिर भी घटनाएँ हैं कि जब-तब सिर उठाती ही रहती हैं। शायद वे भी निकासी चाहती हैं, शायद उन्हें निकासी देकर मैं भी मुक्त हो सकूँ। किंतु घटनाओं के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, न भाषा, न शैली यानी प्रस्तुतीकरण का ढंग जो कुछ जैसा है, बस उसी रूप में मैं इसे प्रस्तुत कर रही हूँ-न कतरब्यौंत, न बनाव-सिंगार।
उतना कुछ सुनकर मैं उस दिन हैरान रह गई थी। इस घर के प्राणियों के साथ इस घर की छत के नीचे रहते मुझे इतना समय हो गया है-तब आज तक इतनी-सी बात का सुराग मुझे क्यों नहीं मिला ? अपने ही बारे में मैं इतनी अनजान कैसे बनी रही ? वह सब कुछ उस क्षण सुनकर मेरा मुँह खुला-का-खुला रह गया, साँस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे।
माँ महीनों से बीमार थीं, उनकी सेवा में रची-बसी मैं पूरे समय खयाल रखती कि माँ को पूरा आराम मिले, उनके मन को किसी तरह की ठेस न पहुँचे। इसके लिए मैं कॉलेज के कामों को जल्दी-से-जल्दी निबटाकर प्रायः रसोई में ही घुसी रहती। घर के सदस्य यानी भाई, चाचा दोनों की माँग-रुचि सब एक-दूसरे से भिन्न होती थी। उनके जाने-आने के समय अलहदा-अलहदा होते थे। माँ का खाना अलग बनता-सादा, हलका, सुपाच्य। चाचा और भैया को कुछ गरिष्ठ मिर्च-मसालेवाला खाना भाता-मैं हर किसी की रुचि का खयाल रखती हुई अपने को सबकी सेवा में रत रखती, फिर भी माँ को प्रसन्न रखना मेरा पहला काम था। उनकी ठीक-ठीक परिचर्या मेरा पहला नियम था, पर कल्याणी मौसी की उस बात ने तो मुझे सब कुछ भुला दिया-उनके जाते ही मैं तुरत-फुरत माँ के पलँग के सामने जाकर खड़ी हो गई, ऐन उनके मुँह के सामने-माँ मेरा चेहरा देख भयभीत हो गई होंगी, उनकी फैल गईं पुतलियों और काँपते हुए होंठों से इसका अनुमान मैं बखूबी लगा पा रही थी।
‘‘माँ !’’ मैंने उस समय मानो प्रयत्नपूर्वक उस शब्द का उच्चारण किया हो। मेरी आवाज में हलका-सा रुदन था।
‘‘मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं अपने बाप की बेटी नहीं हूँ। मेरे पिता क्या चाचा हैं ?’’
माँ के चेहरे का रंग एकाएक उड़ गया था, उनके होंठों से स्वर नहीं फूटा, उनकी आँखें बेहद चौड़ी नजर आ रही थीं, जैसे मेरी बात ने उन्हें एक नए वात्या-चक्र में फेंक दिया हो।
‘‘मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या यह सच है ?’’
‘‘क्यों पूछ रही है तू यह सब ?’’ इतनी-सी देर में माँ ने जैसे साहस बटोर लिया था।
‘‘इतने लंबे समय बाद न !’’
‘‘वही तो।’’
‘‘क्योंकि यह भयंकर बात मुझे इसी क्षण मालूम हुई है, तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातों से।’’
‘‘तो ?’’ माँ मेरी बात समझ रही थीं।
‘‘तो क्या, मैं अब जिंदा नहीं रहूँगी। इस एक छोटे-से क्षण में ही मैं अपनी आँखों में कितना गिर गई हूँ, मैं ही जानती हूँ।’’ और मैं फूट-फूटकर रोने लगी थी।
‘‘जिंदा तो मुझे नहीं रहना चाहिए था, अपनी आँखों में तो मुझे गिर जाना चाहिए था, बेटी !’’
‘‘मत कहो मुझे बेटी !’’ मैं दहाड़ी थी।
‘‘चल न सही, पर मैं तुझे समझाती हूँ।’’ शायद माँ ने मेरी आँखों में एक विचित्र प्रकार के निश्चय को पढ़ लिया था। ‘‘आज से अठारह वर्ष पहले ही मुझे मर जाना चाहिए था, पर नहीं मरी तुम बच्चों के कारण ही और तू अब कह रही है कि तू जिंदा नहीं रहेगी।’’
‘बेटी’ शब्द उचारने से उन्होंने अपने को इस बार बचा लिया था और नए सिरे से एक दूसरा वाक्य बनाया, ‘‘देखो, ज़िंदगी एक सीधी-सरल रेखा नहीं हुआ करती है, इसके बीच में दसियों क्या हजारों उतार-चढ़ाव आते हैं, सिर्फ आदमी को रुलानेवाले ही नहीं, कई बार बेहद अनचाहे, खतरनाक हादसे भी घटते हैं, आदमी को फिर भी जीना पड़ता है, तेरी माँ की जिंदगी में भी बहुत कुछ घटित हुआ है, मेरी हालत तू देख ही रही है, फिर भी मैं जिंदा हूँ।’’
‘‘तुम्हें सचमुच मर जाना चाहिए था, माँ, तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। तुम हम भाई-बहनों की वजह से क्यों जिंदा रहीं ? हमें भी तुम अपने साथ ही मार डालतीं, यह और अच्छा होता। यही होना चाहिए था।’’
मेरी आवाज रुँध गई थी, होंठ कँपकँपाकर रह गए थे, मैं माँ के पास से भाग जाना चाहती थी, पर माँ में उस समय न जाने कहाँ से ताकत आ गई थी, मेरा हाथ उन्होंने लपककर थाम लिया था, ‘‘मेरी बात तो सुन, इधर आ मेरे पास।’’
मेरी माँ ने घसीटकर मुझे बिस्तर पर अपने साथ बैठा लिया था और अपनी कहानी सुनाने लगी थीं-
‘‘अभी तक तू नासमझ थी। अब वह समय आ गया है, जब मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, मुश्किल से मैं पंद्रह साल की रही होऊँगी। तेरे बाबूजी उस समय मुझसे तीन गुनी उम्र के थे। देह काफी कुछ ढल चुकी थी, मन शायद उससे भी ज्यादा। तेरे नानाजी ने मुझ जैसी कमसिन कली को उस बैल सरीखे आदमी के साथ क्यों बाँध दिया था, वह मैं जानती हूँ। जिस घर में नौ खाय तेरह की भूख बनी रहती हो, उस घर की लड़कियों को जहाँ-तहाँ ऐसे ही डाला जाता है। तेरे नानाजी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वह मुझे एक अच्छे खाते-पीते घर में देना चाहते थे। हर पिता की यही कामना रहती है। वह सोचते थे, अगर उनकी बेटी आज तक अपने घर में अच्छा खा-पहन नहीं सकी तो न सही, कम-से-कम आगे तो वह रोटी-कपड़े से महरूम न रहे। आदमी बड़ी उम्र का होने से क्या होता है, वह उसे लाड़-चाव से रखेगा, महलों का सुख तो भोग सकेगी वह।
‘‘कहाँ जानते थे वह कि उन्होंने अपनी बेटी को महल में नहीं, एक मकबरे में कैद कर दिया है। मकबरा जैसा उदास, सूना और वीरान होता है, वैसे ही सूने-वीरान थे तेरे बाबू। जो दौलत उनके पास थी वह जुए और सट्टे की कमाई थी। ऐसी कमाई आदमी को कई दूसरी लतों में भी फँसा देती है। औरत उनके लिए महज एक मजाक थी, नशा उतरा नहीं कि औरत भी मिट्टी की हाँडी की तरह उनकी आँखों से उतर जाती थी। औरत यानी मैं। तेरे बाबू जितना कमाते उतना ही शराब में गारत कर देते। घर में कोई बड़ा-बूढ़ा कुछ कहने-सुननेवाला था नहीं। मैं कुछ कहती तो धड़ाधड़ पीटी जाती, अपने सामने वह किसी को कुछ समझते ही न थे।
‘‘उन दिनों तेरे बाबू से नफ़रत होने के साथ-साथ मुझे भय भी लगने लगा था। दो बच्चों की माँ होने के बावजूद मैं तेरे बाबू को छोड़कर अपने बच्चों के साथ कहीं दूर भाग जाना चाहती थी; पर तेरे इन चाचा के कारण ही ठहरी रही। घर की दशा देखकर उन्होंने अपनी बदली इसी शहर के दफ्तर में करवा ली थी, जिससे वह घर को सँभाल सकें। उन्होंने तेरे बाबू को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उनके करतबों में राई-रत्ती अंतर नहीं आया। उन्होंने अपनी हरकतें ज्यों-की-त्यों रखीं। तेरे चाचा के आने से पहले घर में खाने के लाले भी पड़ने लगे थे, तेरे चाचा के आ जाने से समझो घर की लाज रह गई...।’’
‘‘जिसे आगे चलकर तुमने चीर-चीर कर डाला। खैर, आप अपनी बात जारी रखिए।’’ व्यंग्य का एक बड़ा चाबुक मारकर मैंने माँ को आगे बढ़ने के लिए तिक-तिकाया, पर माँ के चेहरे पर तब तक गहरी कालिमा छा चुकी थी, उनके हलक को एक भारी चुप्पी ने घेर लिया था।
‘‘बोलिए न, आगे क्या हुआ, मैं इस भूमंडल पर कैसे अवतरित हुई ?’’
‘‘तू अभी इसे नहीं समझेगी।’’ एक लंबी साँस लेकर मेरे प्रश्न के उत्तर में माँ ने सँभल-सँभलकर कहना शुरू किया, ‘‘जो आदमी घर का सर्वेसर्वा बन जाता है, जर से लेकर जमीन और औरत का स्वामी भी वही होता है। मेरे साथ यही हुआ। मैं अनपढ़ गँवार अपने को बचाकर कहाँ ले जा सकती थी ! तेरे बाबू में तो सट्टे के दाँव को हारते रहने के साथ दूसरे किसी भी दाँव को बचाकर रखने की ताकत नहीं रह गई थी, तेरे चाचा ही अपनी आमदनी से घर चलाते और तुम तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च झेलते। तेरे चाचा ने इसीलिए शादी भी नहीं की। तेरे बाबू तो पूरा घर अपनी आँखों के सामने उजड़ता-बिखरता देखते रहे थे। तेरे चाचा इधर न आते तो मैं सोचती हूँ, एक दिन यह नौबत आ जाती कि हम सब खुद भी एक-दूसरे की हत्या कर खत्म हो जाते...।’’
‘‘वही अच्छा हुआ होता।’’ मैंने माँ को बीच में फिर टोका था।
‘‘चल तेरी समझ इतनी ही है तो इतनी ही सही। तुम छोटी हो, बहुत कुछ समझने की तुम्हारी उम्र अभी है भी नहीं।’’
‘‘नहीं माँ, तुम मुझे बच्ची न समझो, मैं सब कुछ समझती हूँ और तुम्हारी इतनी बातें सुनकर यह भी समझ गई हूँ कि बाबू गाँववाले उस टूटे-फूटे मकान में क्यों हैं ? चाचा और तुम्हारा यह कहना कि उनका मन उधर रहकर खेती में लगता है, एकदम झूठ है। अब यह भी समझी हूँ कि आप लोग दूसरे भाई-बहन के साथ मुझसे मेरे पिता को चाचा क्यों कहलवाते हैं।
‘‘बाकी आज मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि आज से मुझे तुमसे और तुम्हारे इन दूसरे पति से सख्त नफरत हो गई है, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी वह बड़ी पक्की सहेली कल्याणीजी इधर न ही आई होती तो ही अच्छा था। क्यों सुन लीं मैंने आप दोनों की बातें, क्यों तुमने अपनी सहेली के सामने वह सब उगला, जो मुझे नहीं जानना चाहिए था ? क्यों...क्यों...क्योंऽऽ?
तुम्हारी वह कल्याणीजी मेरा कितना कल्याण कर गई हैं, तुम नहीं जानतीं...।’’
मैं उस समय रीछनी बन गई थी, माँ पर झपट्टा मारने के लिए उतारू। शायद यह अच्छा ही हुआ कि उसी समय चाचा कमरे में आ गए। मेरा वह स्वरूप देखकर बोले, ‘‘इसे क्या हुआ है ? यह इतनी बौखलाई क्यों है ? इसकी इस तरह की शक्ल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्यों ?’’
पर इससे पहले कि वह मुझसे कुछ पूछते, माँ कुछ जवाब देतीं, मैं कमरे से बाहर निकल गई थी और अपने कमरे में पहुँचकर कमरे के पार्टीशन की दीवार से आँख लगाकर देखने लगी थी कि अब क्या होता है।
चाचा ने माँ से फिर पूछा था, ‘‘आखिर इसे हुआ क्या ?’’
‘‘सब कुछ तुम्हारा ही किया-धरा है।’’ माँ ने फुंकारा था।
‘‘मेराऽऽ!’’ चाचा हकबकाकर रह गए थे, पर माँ ने उन्हें जिन निगाहों से देखा और उनकी आवाज में जो तुर्शी भरी हुई थी, उसी से लगता था, चाचा वह आक्षेप सुनकर बुरी तरह बौखला गए थे। किसी तरह अपने को साधकर ही उन्होंने दूसरा प्रश्न किया होगा,‘‘कल्याणीजी गईं ?’’
‘‘चली गईं।’’ माँ की आवाज की गहराई और धीमेपन से वह चौंके थे, पर उस समय और कुछ न कहकर उन्होंने इतना ही पूछा था, ‘‘कब गईं वह ?’’
‘‘आधा घंटा पहले।’’
‘‘कैसे ? इधर दो दिन रुकीं और उनके जाने के वक्त हमें खबर भी न हुई।’’
‘‘असीम उन्हें छोड़ने गया है।’’
‘‘अब तुम्हारी तबीयत कैसी है ?’’ चाचा ने प्रकरण बदल दिया था। माँ तकिए पर सिर रखकर सीधी लेट गई थीं। उनकी आँखें आँसुओं से भरी थीं। दरार में से मैं सब कुछ साफ-साफ देख रही थी। पिछवाड़े आसमान में शाम का सितारा उग आया होगा, क्योंकि घर में अँधेरा भर गया था।
‘‘तबीयत से तुम्हें क्या मतलब ?’’ माँ कह रही थीं, ‘‘मुझे तब नहीं मरने दिया, अब मर जाने दो। जवान बेटी माँ का नंगापन जब पूरी तरह देख ले तब माँ को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।’’
‘‘आखिर बात क्या हुई ?’’
‘‘अब भी नहीं समझ रहे हो, मीना की आँखों में भयंकर गुस्से की लाली देखकर भी नहीं ? तुम्हारी मीना जिसे तुम लाड़ से आँखों पर बैठाते थे, वह तुम्हारी सब करतूतें जान गई है।’’
‘‘कैसी करतूतें, मेरी या अपने बाबू की ?’’
‘‘वह सब कुछ भी जान लिया है उसने। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ बताकर उसे शांत कर दूँ, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह और अंगारा बनती चली गई।’’
चाचा क्षण-भर को खामोश हो गए थे, फिर गुम्म-सी आवाज में बोले थे, ‘‘धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।
‘‘तुम गलतफहमी में हो। मैं उसे जानती हूँ, उसको, उसके मन को, उसकी जिद को।’’ माँ जो पूरे महीने-भर से खाट पर पड़ी थीं, उनमें इस तरह करारेपन से बोलने की हिम्मत न जाने कहाँ से आ गई थी, शायद वह अपने और मेरे भविष्य से भयभीत थीं, अंधकारमय भविष्य शायद व्यक्ति को इसी तरह दहला देता है और उस दहल में से ही वह चिनगारी सुलगती है जो उसे चीखने पर मजबूर कर देती है।
माँ ने इस बारे में अपने माथे पर दुहत्थड़ मारते हुए चीखकर कहा था, ‘‘जो हुआ वह तो हुआ। वह सब तो उसके सामने है। पर जो अब होने को है, उसको जानेगी-देखेगी, तब क्या होगा ? अभी तो शुरुआत ही है। उसी से मेरी जान निकली जा रही है। आगे चलकर मेरी क्या दशा होगी और मेरी कौन सेवा करेगा, बोलो न ! मैं अब इस इल्लत को हरगिज नहीं रखूँगी। मैंने कह दिया, कल ही अस्पताल जाकर....।’’
तो क्या माँ अब फिर से किसी पाप को जन्म देनेवाली है-इस सूचना ने मुझे बुरी तरह दहला दिया। मैं एकाएक जोर से चीख पड़ने को ही थी कि मैंने अपने के सँभाल लिया। चाचा के उत्तर को बिना सुने ही उस दरार से अलग हट-कर मैं अपने बिस्तर पर गिरी और फफक-फफककर रोने लगी। इतनी देर दरार से देखने के लिए झुकी-झुकी मेरी कमर पिरा उठी थी।
क्यों होता है ऐसा ? बड़े जन बच्चों पर क्यों जुल्म करते हैं ? और छोटे भी, जिन्हें बड़ों के क्रिया-कलापों से कुछ लेना-देना नहीं होता, उनकी बेजा हरकतें उन्हें क्यों रुलाती हैं ? शायद यही मनोविज्ञान है कि बड़ों की तरह छोटे भी अपने बड़ों से बहुत उम्मीदें लगा बैठते हैं, उन्हें वे पाक-साफ आदर्शवादी देखना चाहते हैं। अपने नहीं, अपने बड़ों के कारनामे उन्हें एक विचित्र झूँझल से भर देते हैं। क्यों होता है ऐसा ? मैं अपने में डूब चली थी और डूबते-डूबते अपने में गुम्म हो गई थी। नींद मुझ पर कब हावी हो गई, मुझे चेत ही नहीं हुआ।
अचानक आँख खुली तो स्वर शांत हो चुके थे, कमरे में पूरी तरह अँधेरा बिछ चुका था। एक अजीब-सा सूनापन था। चारों ओर विराट् शांति बिखरी पड़ी थी। क्या असीम भैया कल्याणी मौसी को गाड़ी पर बिठाकर लौट आया होगा ? लौट तो आया ही होगा, पर लौटकर उसने मुझे क्यों नहीं जगाया ? माँ ने भी मुझे आवाज नहीं लगाई ? माँ पुकारतीं भी तो मैं क्या बोलनेवाली थी ? कभी नहीं। माँ से अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं रह गया है-मैं सोचती रही।
माँ क्या बाबू को समझाकर रास्ते पर नहीं ला सकती थीं ? क्या वह चाचा को लताड़ नहीं सकती थीं ? पर उन पर तो वासना का भूत सवार रहा होगा। सोच की घड़ी मस्तिष्क में फिर घूमने लगी थी। उन्होंने अपने को चाचा के चंगुल में क्यों फँस जाने दिया ? अपना आगा-पीछा क्यों नहीं सोचा ? मोहल्लेवाले तो यही जानते हैं कि हम तीनों बच्चे बाबू के ही हैं; माँ बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में रहती हैं और बाबू खेती-बाड़ी के लिए गाँव में। चाचा ने शादी नहीं की, न सही। चौथे की बात मन में आते ही मेरा मन एक विचित्र कड़वाहट से भर गया। नहीं, मैं इस चौथे को नहीं आने दूँगी। माँ को और उसको दोनों को खत्म कर दूँगी, किसी भी....।
मैं खराब गंदी माँ की बेटी हूँ, इसलिए यही करूँगी। ताज्जुब तो यह है कि चाचा के कुकर्म अभी तक जारी हैं। पर वह सब मैं इससे पहले कहाँ जानती थी। इतने लंबे समय तक मैं अनजान बनी रही, आश्चर्य है। कल्याणी मौसी ने ही तो माँ को नसीहत दी थी, ‘‘एक बच्ची अब इस बाप से हुई तो हुई, पर अगर यही सिलसिला रहा तो तेरे पाप के ढोल से एक दिन मोहल्लेवाले जरूर वाकिफ हो जाएँगे। हीरालाल भले ही गाँव से आते-जाते रहें, पर लोगों की नजरें काफी पैनी होती हैं। यह तू भी समझ और अपने इस देवर को भी समझा। बच्चों पर भी इसका असर अच्छा नहीं पड़ता। एक बात तू यह अच्छी तरह यह समझ ले कि माँ-बाप के इस तरह के खिलवाड़ बच्चों को नहीं सुहाते।’’
नहीं, आत्मकथा लिखने के लिए मेरे विचार में एक तीसरी चीज और जरूरी है, ईमानदारी और सचाई। लोग प्रायः अपने को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं, जो कुछ हुआ है, उसे मोड़-तोड़कर रखने की कोशिश करते हैं जिससे वे सुर्खरू भी बने रहें और आत्मकथा लिखने जैसी ख्याति भी अर्जित कर लें-अपनी यह आपबीती खुलकर लिखने में मुझे कोई दरेग नहीं है, मैं ऐसा कोई बड़ा व्यक्तित्व भी तो नहीं, जिसे समाज का भय हो, फिर उन घटनाओं को घटित हुए भी आज अर्सा बीत गया है, अपने इस नए जीवन में प्रविष्ट हुए भी मुझे आठ वर्ष से ऊपर हो गए हैं, मैं अब पूरी पक्की गृहस्थिन हो चुकी हूँ; फिर भी घटनाएँ हैं कि जब-तब सिर उठाती ही रहती हैं। शायद वे भी निकासी चाहती हैं, शायद उन्हें निकासी देकर मैं भी मुक्त हो सकूँ। किंतु घटनाओं के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, न भाषा, न शैली यानी प्रस्तुतीकरण का ढंग जो कुछ जैसा है, बस उसी रूप में मैं इसे प्रस्तुत कर रही हूँ-न कतरब्यौंत, न बनाव-सिंगार।
उतना कुछ सुनकर मैं उस दिन हैरान रह गई थी। इस घर के प्राणियों के साथ इस घर की छत के नीचे रहते मुझे इतना समय हो गया है-तब आज तक इतनी-सी बात का सुराग मुझे क्यों नहीं मिला ? अपने ही बारे में मैं इतनी अनजान कैसे बनी रही ? वह सब कुछ उस क्षण सुनकर मेरा मुँह खुला-का-खुला रह गया, साँस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे।
माँ महीनों से बीमार थीं, उनकी सेवा में रची-बसी मैं पूरे समय खयाल रखती कि माँ को पूरा आराम मिले, उनके मन को किसी तरह की ठेस न पहुँचे। इसके लिए मैं कॉलेज के कामों को जल्दी-से-जल्दी निबटाकर प्रायः रसोई में ही घुसी रहती। घर के सदस्य यानी भाई, चाचा दोनों की माँग-रुचि सब एक-दूसरे से भिन्न होती थी। उनके जाने-आने के समय अलहदा-अलहदा होते थे। माँ का खाना अलग बनता-सादा, हलका, सुपाच्य। चाचा और भैया को कुछ गरिष्ठ मिर्च-मसालेवाला खाना भाता-मैं हर किसी की रुचि का खयाल रखती हुई अपने को सबकी सेवा में रत रखती, फिर भी माँ को प्रसन्न रखना मेरा पहला काम था। उनकी ठीक-ठीक परिचर्या मेरा पहला नियम था, पर कल्याणी मौसी की उस बात ने तो मुझे सब कुछ भुला दिया-उनके जाते ही मैं तुरत-फुरत माँ के पलँग के सामने जाकर खड़ी हो गई, ऐन उनके मुँह के सामने-माँ मेरा चेहरा देख भयभीत हो गई होंगी, उनकी फैल गईं पुतलियों और काँपते हुए होंठों से इसका अनुमान मैं बखूबी लगा पा रही थी।
‘‘माँ !’’ मैंने उस समय मानो प्रयत्नपूर्वक उस शब्द का उच्चारण किया हो। मेरी आवाज में हलका-सा रुदन था।
‘‘मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं अपने बाप की बेटी नहीं हूँ। मेरे पिता क्या चाचा हैं ?’’
माँ के चेहरे का रंग एकाएक उड़ गया था, उनके होंठों से स्वर नहीं फूटा, उनकी आँखें बेहद चौड़ी नजर आ रही थीं, जैसे मेरी बात ने उन्हें एक नए वात्या-चक्र में फेंक दिया हो।
‘‘मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या यह सच है ?’’
‘‘क्यों पूछ रही है तू यह सब ?’’ इतनी-सी देर में माँ ने जैसे साहस बटोर लिया था।
‘‘इतने लंबे समय बाद न !’’
‘‘वही तो।’’
‘‘क्योंकि यह भयंकर बात मुझे इसी क्षण मालूम हुई है, तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातों से।’’
‘‘तो ?’’ माँ मेरी बात समझ रही थीं।
‘‘तो क्या, मैं अब जिंदा नहीं रहूँगी। इस एक छोटे-से क्षण में ही मैं अपनी आँखों में कितना गिर गई हूँ, मैं ही जानती हूँ।’’ और मैं फूट-फूटकर रोने लगी थी।
‘‘जिंदा तो मुझे नहीं रहना चाहिए था, अपनी आँखों में तो मुझे गिर जाना चाहिए था, बेटी !’’
‘‘मत कहो मुझे बेटी !’’ मैं दहाड़ी थी।
‘‘चल न सही, पर मैं तुझे समझाती हूँ।’’ शायद माँ ने मेरी आँखों में एक विचित्र प्रकार के निश्चय को पढ़ लिया था। ‘‘आज से अठारह वर्ष पहले ही मुझे मर जाना चाहिए था, पर नहीं मरी तुम बच्चों के कारण ही और तू अब कह रही है कि तू जिंदा नहीं रहेगी।’’
‘बेटी’ शब्द उचारने से उन्होंने अपने को इस बार बचा लिया था और नए सिरे से एक दूसरा वाक्य बनाया, ‘‘देखो, ज़िंदगी एक सीधी-सरल रेखा नहीं हुआ करती है, इसके बीच में दसियों क्या हजारों उतार-चढ़ाव आते हैं, सिर्फ आदमी को रुलानेवाले ही नहीं, कई बार बेहद अनचाहे, खतरनाक हादसे भी घटते हैं, आदमी को फिर भी जीना पड़ता है, तेरी माँ की जिंदगी में भी बहुत कुछ घटित हुआ है, मेरी हालत तू देख ही रही है, फिर भी मैं जिंदा हूँ।’’
‘‘तुम्हें सचमुच मर जाना चाहिए था, माँ, तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। तुम हम भाई-बहनों की वजह से क्यों जिंदा रहीं ? हमें भी तुम अपने साथ ही मार डालतीं, यह और अच्छा होता। यही होना चाहिए था।’’
मेरी आवाज रुँध गई थी, होंठ कँपकँपाकर रह गए थे, मैं माँ के पास से भाग जाना चाहती थी, पर माँ में उस समय न जाने कहाँ से ताकत आ गई थी, मेरा हाथ उन्होंने लपककर थाम लिया था, ‘‘मेरी बात तो सुन, इधर आ मेरे पास।’’
मेरी माँ ने घसीटकर मुझे बिस्तर पर अपने साथ बैठा लिया था और अपनी कहानी सुनाने लगी थीं-
‘‘अभी तक तू नासमझ थी। अब वह समय आ गया है, जब मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, मुश्किल से मैं पंद्रह साल की रही होऊँगी। तेरे बाबूजी उस समय मुझसे तीन गुनी उम्र के थे। देह काफी कुछ ढल चुकी थी, मन शायद उससे भी ज्यादा। तेरे नानाजी ने मुझ जैसी कमसिन कली को उस बैल सरीखे आदमी के साथ क्यों बाँध दिया था, वह मैं जानती हूँ। जिस घर में नौ खाय तेरह की भूख बनी रहती हो, उस घर की लड़कियों को जहाँ-तहाँ ऐसे ही डाला जाता है। तेरे नानाजी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वह मुझे एक अच्छे खाते-पीते घर में देना चाहते थे। हर पिता की यही कामना रहती है। वह सोचते थे, अगर उनकी बेटी आज तक अपने घर में अच्छा खा-पहन नहीं सकी तो न सही, कम-से-कम आगे तो वह रोटी-कपड़े से महरूम न रहे। आदमी बड़ी उम्र का होने से क्या होता है, वह उसे लाड़-चाव से रखेगा, महलों का सुख तो भोग सकेगी वह।
‘‘कहाँ जानते थे वह कि उन्होंने अपनी बेटी को महल में नहीं, एक मकबरे में कैद कर दिया है। मकबरा जैसा उदास, सूना और वीरान होता है, वैसे ही सूने-वीरान थे तेरे बाबू। जो दौलत उनके पास थी वह जुए और सट्टे की कमाई थी। ऐसी कमाई आदमी को कई दूसरी लतों में भी फँसा देती है। औरत उनके लिए महज एक मजाक थी, नशा उतरा नहीं कि औरत भी मिट्टी की हाँडी की तरह उनकी आँखों से उतर जाती थी। औरत यानी मैं। तेरे बाबू जितना कमाते उतना ही शराब में गारत कर देते। घर में कोई बड़ा-बूढ़ा कुछ कहने-सुननेवाला था नहीं। मैं कुछ कहती तो धड़ाधड़ पीटी जाती, अपने सामने वह किसी को कुछ समझते ही न थे।
‘‘उन दिनों तेरे बाबू से नफ़रत होने के साथ-साथ मुझे भय भी लगने लगा था। दो बच्चों की माँ होने के बावजूद मैं तेरे बाबू को छोड़कर अपने बच्चों के साथ कहीं दूर भाग जाना चाहती थी; पर तेरे इन चाचा के कारण ही ठहरी रही। घर की दशा देखकर उन्होंने अपनी बदली इसी शहर के दफ्तर में करवा ली थी, जिससे वह घर को सँभाल सकें। उन्होंने तेरे बाबू को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उनके करतबों में राई-रत्ती अंतर नहीं आया। उन्होंने अपनी हरकतें ज्यों-की-त्यों रखीं। तेरे चाचा के आने से पहले घर में खाने के लाले भी पड़ने लगे थे, तेरे चाचा के आ जाने से समझो घर की लाज रह गई...।’’
‘‘जिसे आगे चलकर तुमने चीर-चीर कर डाला। खैर, आप अपनी बात जारी रखिए।’’ व्यंग्य का एक बड़ा चाबुक मारकर मैंने माँ को आगे बढ़ने के लिए तिक-तिकाया, पर माँ के चेहरे पर तब तक गहरी कालिमा छा चुकी थी, उनके हलक को एक भारी चुप्पी ने घेर लिया था।
‘‘बोलिए न, आगे क्या हुआ, मैं इस भूमंडल पर कैसे अवतरित हुई ?’’
‘‘तू अभी इसे नहीं समझेगी।’’ एक लंबी साँस लेकर मेरे प्रश्न के उत्तर में माँ ने सँभल-सँभलकर कहना शुरू किया, ‘‘जो आदमी घर का सर्वेसर्वा बन जाता है, जर से लेकर जमीन और औरत का स्वामी भी वही होता है। मेरे साथ यही हुआ। मैं अनपढ़ गँवार अपने को बचाकर कहाँ ले जा सकती थी ! तेरे बाबू में तो सट्टे के दाँव को हारते रहने के साथ दूसरे किसी भी दाँव को बचाकर रखने की ताकत नहीं रह गई थी, तेरे चाचा ही अपनी आमदनी से घर चलाते और तुम तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च झेलते। तेरे चाचा ने इसीलिए शादी भी नहीं की। तेरे बाबू तो पूरा घर अपनी आँखों के सामने उजड़ता-बिखरता देखते रहे थे। तेरे चाचा इधर न आते तो मैं सोचती हूँ, एक दिन यह नौबत आ जाती कि हम सब खुद भी एक-दूसरे की हत्या कर खत्म हो जाते...।’’
‘‘वही अच्छा हुआ होता।’’ मैंने माँ को बीच में फिर टोका था।
‘‘चल तेरी समझ इतनी ही है तो इतनी ही सही। तुम छोटी हो, बहुत कुछ समझने की तुम्हारी उम्र अभी है भी नहीं।’’
‘‘नहीं माँ, तुम मुझे बच्ची न समझो, मैं सब कुछ समझती हूँ और तुम्हारी इतनी बातें सुनकर यह भी समझ गई हूँ कि बाबू गाँववाले उस टूटे-फूटे मकान में क्यों हैं ? चाचा और तुम्हारा यह कहना कि उनका मन उधर रहकर खेती में लगता है, एकदम झूठ है। अब यह भी समझी हूँ कि आप लोग दूसरे भाई-बहन के साथ मुझसे मेरे पिता को चाचा क्यों कहलवाते हैं।
‘‘बाकी आज मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि आज से मुझे तुमसे और तुम्हारे इन दूसरे पति से सख्त नफरत हो गई है, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी वह बड़ी पक्की सहेली कल्याणीजी इधर न ही आई होती तो ही अच्छा था। क्यों सुन लीं मैंने आप दोनों की बातें, क्यों तुमने अपनी सहेली के सामने वह सब उगला, जो मुझे नहीं जानना चाहिए था ? क्यों...क्यों...क्योंऽऽ?
तुम्हारी वह कल्याणीजी मेरा कितना कल्याण कर गई हैं, तुम नहीं जानतीं...।’’
मैं उस समय रीछनी बन गई थी, माँ पर झपट्टा मारने के लिए उतारू। शायद यह अच्छा ही हुआ कि उसी समय चाचा कमरे में आ गए। मेरा वह स्वरूप देखकर बोले, ‘‘इसे क्या हुआ है ? यह इतनी बौखलाई क्यों है ? इसकी इस तरह की शक्ल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्यों ?’’
पर इससे पहले कि वह मुझसे कुछ पूछते, माँ कुछ जवाब देतीं, मैं कमरे से बाहर निकल गई थी और अपने कमरे में पहुँचकर कमरे के पार्टीशन की दीवार से आँख लगाकर देखने लगी थी कि अब क्या होता है।
चाचा ने माँ से फिर पूछा था, ‘‘आखिर इसे हुआ क्या ?’’
‘‘सब कुछ तुम्हारा ही किया-धरा है।’’ माँ ने फुंकारा था।
‘‘मेराऽऽ!’’ चाचा हकबकाकर रह गए थे, पर माँ ने उन्हें जिन निगाहों से देखा और उनकी आवाज में जो तुर्शी भरी हुई थी, उसी से लगता था, चाचा वह आक्षेप सुनकर बुरी तरह बौखला गए थे। किसी तरह अपने को साधकर ही उन्होंने दूसरा प्रश्न किया होगा,‘‘कल्याणीजी गईं ?’’
‘‘चली गईं।’’ माँ की आवाज की गहराई और धीमेपन से वह चौंके थे, पर उस समय और कुछ न कहकर उन्होंने इतना ही पूछा था, ‘‘कब गईं वह ?’’
‘‘आधा घंटा पहले।’’
‘‘कैसे ? इधर दो दिन रुकीं और उनके जाने के वक्त हमें खबर भी न हुई।’’
‘‘असीम उन्हें छोड़ने गया है।’’
‘‘अब तुम्हारी तबीयत कैसी है ?’’ चाचा ने प्रकरण बदल दिया था। माँ तकिए पर सिर रखकर सीधी लेट गई थीं। उनकी आँखें आँसुओं से भरी थीं। दरार में से मैं सब कुछ साफ-साफ देख रही थी। पिछवाड़े आसमान में शाम का सितारा उग आया होगा, क्योंकि घर में अँधेरा भर गया था।
‘‘तबीयत से तुम्हें क्या मतलब ?’’ माँ कह रही थीं, ‘‘मुझे तब नहीं मरने दिया, अब मर जाने दो। जवान बेटी माँ का नंगापन जब पूरी तरह देख ले तब माँ को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।’’
‘‘आखिर बात क्या हुई ?’’
‘‘अब भी नहीं समझ रहे हो, मीना की आँखों में भयंकर गुस्से की लाली देखकर भी नहीं ? तुम्हारी मीना जिसे तुम लाड़ से आँखों पर बैठाते थे, वह तुम्हारी सब करतूतें जान गई है।’’
‘‘कैसी करतूतें, मेरी या अपने बाबू की ?’’
‘‘वह सब कुछ भी जान लिया है उसने। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ बताकर उसे शांत कर दूँ, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह और अंगारा बनती चली गई।’’
चाचा क्षण-भर को खामोश हो गए थे, फिर गुम्म-सी आवाज में बोले थे, ‘‘धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।
‘‘तुम गलतफहमी में हो। मैं उसे जानती हूँ, उसको, उसके मन को, उसकी जिद को।’’ माँ जो पूरे महीने-भर से खाट पर पड़ी थीं, उनमें इस तरह करारेपन से बोलने की हिम्मत न जाने कहाँ से आ गई थी, शायद वह अपने और मेरे भविष्य से भयभीत थीं, अंधकारमय भविष्य शायद व्यक्ति को इसी तरह दहला देता है और उस दहल में से ही वह चिनगारी सुलगती है जो उसे चीखने पर मजबूर कर देती है।
माँ ने इस बारे में अपने माथे पर दुहत्थड़ मारते हुए चीखकर कहा था, ‘‘जो हुआ वह तो हुआ। वह सब तो उसके सामने है। पर जो अब होने को है, उसको जानेगी-देखेगी, तब क्या होगा ? अभी तो शुरुआत ही है। उसी से मेरी जान निकली जा रही है। आगे चलकर मेरी क्या दशा होगी और मेरी कौन सेवा करेगा, बोलो न ! मैं अब इस इल्लत को हरगिज नहीं रखूँगी। मैंने कह दिया, कल ही अस्पताल जाकर....।’’
तो क्या माँ अब फिर से किसी पाप को जन्म देनेवाली है-इस सूचना ने मुझे बुरी तरह दहला दिया। मैं एकाएक जोर से चीख पड़ने को ही थी कि मैंने अपने के सँभाल लिया। चाचा के उत्तर को बिना सुने ही उस दरार से अलग हट-कर मैं अपने बिस्तर पर गिरी और फफक-फफककर रोने लगी। इतनी देर दरार से देखने के लिए झुकी-झुकी मेरी कमर पिरा उठी थी।
क्यों होता है ऐसा ? बड़े जन बच्चों पर क्यों जुल्म करते हैं ? और छोटे भी, जिन्हें बड़ों के क्रिया-कलापों से कुछ लेना-देना नहीं होता, उनकी बेजा हरकतें उन्हें क्यों रुलाती हैं ? शायद यही मनोविज्ञान है कि बड़ों की तरह छोटे भी अपने बड़ों से बहुत उम्मीदें लगा बैठते हैं, उन्हें वे पाक-साफ आदर्शवादी देखना चाहते हैं। अपने नहीं, अपने बड़ों के कारनामे उन्हें एक विचित्र झूँझल से भर देते हैं। क्यों होता है ऐसा ? मैं अपने में डूब चली थी और डूबते-डूबते अपने में गुम्म हो गई थी। नींद मुझ पर कब हावी हो गई, मुझे चेत ही नहीं हुआ।
अचानक आँख खुली तो स्वर शांत हो चुके थे, कमरे में पूरी तरह अँधेरा बिछ चुका था। एक अजीब-सा सूनापन था। चारों ओर विराट् शांति बिखरी पड़ी थी। क्या असीम भैया कल्याणी मौसी को गाड़ी पर बिठाकर लौट आया होगा ? लौट तो आया ही होगा, पर लौटकर उसने मुझे क्यों नहीं जगाया ? माँ ने भी मुझे आवाज नहीं लगाई ? माँ पुकारतीं भी तो मैं क्या बोलनेवाली थी ? कभी नहीं। माँ से अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं रह गया है-मैं सोचती रही।
माँ क्या बाबू को समझाकर रास्ते पर नहीं ला सकती थीं ? क्या वह चाचा को लताड़ नहीं सकती थीं ? पर उन पर तो वासना का भूत सवार रहा होगा। सोच की घड़ी मस्तिष्क में फिर घूमने लगी थी। उन्होंने अपने को चाचा के चंगुल में क्यों फँस जाने दिया ? अपना आगा-पीछा क्यों नहीं सोचा ? मोहल्लेवाले तो यही जानते हैं कि हम तीनों बच्चे बाबू के ही हैं; माँ बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में रहती हैं और बाबू खेती-बाड़ी के लिए गाँव में। चाचा ने शादी नहीं की, न सही। चौथे की बात मन में आते ही मेरा मन एक विचित्र कड़वाहट से भर गया। नहीं, मैं इस चौथे को नहीं आने दूँगी। माँ को और उसको दोनों को खत्म कर दूँगी, किसी भी....।
मैं खराब गंदी माँ की बेटी हूँ, इसलिए यही करूँगी। ताज्जुब तो यह है कि चाचा के कुकर्म अभी तक जारी हैं। पर वह सब मैं इससे पहले कहाँ जानती थी। इतने लंबे समय तक मैं अनजान बनी रही, आश्चर्य है। कल्याणी मौसी ने ही तो माँ को नसीहत दी थी, ‘‘एक बच्ची अब इस बाप से हुई तो हुई, पर अगर यही सिलसिला रहा तो तेरे पाप के ढोल से एक दिन मोहल्लेवाले जरूर वाकिफ हो जाएँगे। हीरालाल भले ही गाँव से आते-जाते रहें, पर लोगों की नजरें काफी पैनी होती हैं। यह तू भी समझ और अपने इस देवर को भी समझा। बच्चों पर भी इसका असर अच्छा नहीं पड़ता। एक बात तू यह अच्छी तरह यह समझ ले कि माँ-बाप के इस तरह के खिलवाड़ बच्चों को नहीं सुहाते।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i